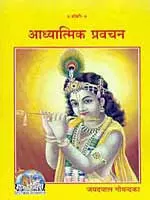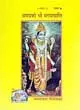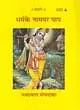|
गीता प्रेस, गोरखपुर >> आध्यात्मिक प्रवचन आध्यात्मिक प्रवचनजयदयाल गोयन्दका
|
443 पाठक हैं |
||||||
इस पुस्तिका में संग्रहीत स्वामीजी महाराज के प्रवचन आध्यात्म,भक्ति एवं सेवा-मार्ग के लिए दशा-निर्देशन और पाथेय का काम करेंगे।
धर्म और नीति
श्रीज्वालाप्रसादजी डिप्टी कलेक्टर ने क्रोधकी अपनी बीती हुई घटना सुनायी। घरमें नौकरको क्रोधसे धमकाया गया। काम तो बन गया पर स्थिति बिगड़ गयी। इस विषयमें उनके प्रश्नका उत्तर-
नौकरके हितके लिये क्रोध तो लाना चाहिये, पर बनावटी, असली नहीं। असली क्रोध आयेगा तो हमपर सवार होकर हमारी दुर्दशा कर देगा। यदि बनावटी क्रोध न ला सके तो काम भले ही देरसे हो या बिगड़ जाय पर क्रोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि अगर हम क्रोध करेंगे और यदि क्रोधके वश में हो गये तो हमारा आध्यात्मिक पतन हो जायगा। क्रोध न करना इसके लिये ही उपदेश दिया जाता है। क्रोध करो इसके लिये उपदेशकी आवश्यकता ही नहीं है; क्योंकि प्राय: जीवोंकी आदत बिगड़ी हुई है। एक भाई कहता है कि नकली क्रोध करनेसे असली आ जाता है, हम उसके वशीभूत हो जाते हैं तो ऐसी स्थितिमें उसे क्रोध नहीं करना चाहिये। मनके प्रतिकूल जितनी क्रिया हो रही है वह अनिच्छा या परेच्छासे हो रही है। मालिककी राजीमें हम राजी रहें। प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मालिक जो भी मनके विरुद्ध करें उसमें क्रोध न हो, शान्ति बनी रहे। वही मालिकका भक्त है, अन्यथा कथनमात्रकी भक्ति है। मनुष्यका स्वभाव अलग-अलग है। मेरे काममें चार नीति हैं-साम, दाम, दण्ड, भेद। मैं पहले साम, दामको काममें लेता हूँ। इनसे काम न चले तो दण्डको काममें लेता हूँ भेदका काम बहुत ही कम सालमें एकदो बार पड़ता है। साम-समझाकर प्रेमसे, दाम-लोभ स्वार्थ दिखाकर, दण्ड-भय दिखाकर, बनावटी क्रोध दिखाकर, भेद-खूफिया पुलिसकी तरह। यह चौथी भेदनीति सबसे नीचे दर्जेकी बात है, जहाँतक हो इसको काममें नहीं लाना चाहिये। साधु पुरुषोंके लिये ऊँचा-नीचा दर्जा कोई नहीं है, वे कभी कोई अनुचित क्रिया करते ही नहीं। उनकी प्रत्येक क्रिया आदर्श होते हुए भी हमारे लिये जो बात वे कहें, हमारे लिये वही करना श्रेष्ठ है। महात्मापर क्रोधका असर नहीं होता। इसीलिये ही उनके लिये कहा गया है- समरथको नहीं दोष गुसाड़। उनपर क्रोधका असर नहीं होता। हम अपनेको वश में नहीं रख सकते, इसलिये महात्मा लोगोंके अनुसार आचरण न करके वे जैसी आज्ञा दें उसीके अनुसार करना चाहिये। जैसे महात्माने ३० वर्षकी अवस्थामें विवाह नहीं किया वह आदर्श है, पर दूसरेने ३० वर्षकी अवस्थामें उनकी नकल करनी चाही, कहा कि तुम विवाह कर लो। वे जैसा कहें वही करना चाहिये। नीति और धर्मकी व्याख्या- जयदेव कविकी एक राजाने काफी धन दिया। रास्तेमें डाकुओंने उनके हाथ काटकर एक सूखे कुंएमें डाल दिया तथा धन लूटकर ले गये। उस राजाने जंगलसे जाते समय कीर्तन-ध्वनि सुनकर उन्हें निकाला और अपने साथ ले गये। एक बार वे डाकू पकड़े गये एवं दरबारमें लाये गये। जयदेवजीने काफी धन दिलवाकर उन्हें छुड़वा दिया। रास्तेमें कोतवालने पूछा कि भक्तजीकी आपके ऊपर इतनी कृपा क्यों है? उन्होंने कहा कि वह हमारा साथी है हम इसकी पोल न खोल दें इसलिये इसने हमें धन दिलाया है। इतना कहते ही धरती फट गयी और चारों डाकू उसीमें समा गये। मेरेसे तो ऐसा काम पड़नेपर इस तरहका व्यवहार नहीं होता।
आखिर में नतीजा क्या हुआ चारों मारे गये। उस नीतिका परिणाम तो यही हुआ। जिस साधुतासे उनकी मृत्यु हो जाय, उस साधुतामें धब्बा लगाकर भी उनकी जान बच जाती तो उससे भी अच्छा था। उनका हित कैसे ही यह भाव ही हृदयमें रखना चाहिये। जयदेव कविका व्यवहार, भाव सबकी प्रशंसा ही की जाती है। उनको किसी प्रकारका दोष नहीं लगाते हैं, पर इससे भी बढ़कर दूसरी नीति हो सकती है। साधुकी साधु ही जानें। महात्माको किस प्रकार करना चाहिये यह हम नियत नहीं कर सकते। उसका हित कैसे ही यही भाव दृढ़ करना चाहिये। दण्डका नम्बर तीसरा ही है, पर हम नहीं कह सकते कि महात्मा उसको काम में ले ही नहीं। उनके लिये हम कोई विधान नहीं कर सकते। उनका तो सारी दुनियापर लक्ष्य है वे सबके लिये धर्म और नीतिका ख्याल करते हैं। जो कुछ क्रिया करनी है वह इसी उद्देश्यसे करनी चाहिये कि उसका हित कैसे हो। रागद्वेषके वशीभूत होकर नहीं करना चाहिये। ऐसा तो कोई एक ही निकलता है जो रागद्वेषके वशीभूत न हो। यदि वास्तव में आपका भाव ठीक है तो सत्य तो सत्य ही है। कभी-न-कभी उसमें यह भाव आयेगा ही कि वे मेरा हित ही चाहते थे, मेरी ही भूल थी। मेरे साथमें बुराई करनेपर भी बदलेमें यदि मेरे द्वारा उसकी हितकी क्रिया होगी तो आखिर में उसको समझ आयेगी ही। यदि नहीं भी आये तो कोई परवाह नहीं अपने तो हितकी ही चेष्टा करते रहना चाहिये। उसको यदि चेत कराना हो तो उसके हितकी विशेष चेष्टा करो, अपनी आत्माको जोरदार बनाओ। हृदयमें यह भाव रखो कि उसका हित हो, उसका हित चाहते रहो इसका भी असर पड़ेगा। यदि हम वास्तव में किसीका हित चाहते हों तो साम, दाम, दण्ड, भेद सबका ही उपयोग कर सकते हैं। पहले साम, दाम, दण्ड फिर भेद-यही इसका क्रम है। संन्यास आश्रममें जहाँतक हो साधुताका ही व्यवहार करना है, उसे कोई शासन तो करना है नहीं। अपने स्वार्थके लिये अच्छे पुरुष भेद नीति काम में नहीं लाते।
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥
(गीता ४।१६)
कर्म क्या है? और अकर्म क्या है?-इस प्रकार इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिये वह कर्मतत्त्व मैं तुझे भलीभाँति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात् कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा।
प्रश्व-इस श्लोकका क्या भाव है?
उत्तर-देखनेमें कर्म होते हुए भी वास्तवमें अकर्म होते हैं। देखनेमें अकर्म होते हुए भी वास्तव में कर्म हैं। इस विषयमें विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं। इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। साधारण लोग तो क्रियाको कर्म मान लेते हैं और चुप रहनेको, कुछ न करनेकी अकर्म मान लेते हैं। पर गीता २।७१ के अनुसार सब क्रिया करते हुए भी वह अकर्म ही है, वह कर्ता अकर्ता ही है। उनमें कोई कामना नहीं, परवाह नहीं, आसक्ति नहीं, अहंकार नहीं, वह सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है। दूसरा आसन लगाकर समाधिमें बैठा है पर यदि वह दम्भी है तो कर्ता है ही।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते।।
(गीता ३।६)
जो मूढ़बुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंकी हठपूर्वक ऊपरसे रोककर मनसे इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी कहा जाता है।
हनुमान् जी सरीखे बुद्धिमान् को कालनेमिने ठग लिया। अकर्ता बनकर दम्भ करता है। हनुमान् जी विद्वान् थे, भक्त थे, कवि थे, व्याकरण जाननेवाले थे, पर मोहित हो गये। कालनेमि देखनेमें अकर्ता दीखनेपर भी वास्तव में दम्भी पापाचारी था।
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः।।
(गीता ४।२०)
जो पुरुष समस्त कर्मोंमें और उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्यतृप्त है, वह कर्मोंमें भलीभाँति बर्तता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता।
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते।
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते।।
(गीता १८।१७)
जिस पुरुषके अन्त:करणमें 'मैं कर्ता हूँ" ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसरिक पद्धाथों में कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पापसे बँधता है।
देखनेमें मारकाटकी क्रिया होते हुए भी वह अकर्ता ही है। मारकाट देखकर ही साधारण लोग कर्ता मान लेते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है, कर्म-अकर्मका रहस्य इतना गहन है कि विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं। भगवान् के चरित्र आचरणोंको देखकर ऋषिलोग भी मोहित हो जाते थे। यह बात तुम्हारे समझमें आ जायगी तो तुम मुक्त हो जाओगे। कर्म तत्त्व भगवान् ने बताया है-
कर्मण्यकर्म यः पशयेदकर्मणि च कर्म यः।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्॥
(गीता ४।१८)
जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान् है और वह योगी समस्त कर्मोंको करनेवाला है।
प्रश्व-महापुरुषसे प्रश्रोत्तर करना ठीक है या नहीं।
उत्तर-ठीक है भी और नहीं भी। श्रद्धासे जिज्ञासु होकर तत्त्व जाननेके लिये पूछा जाय वह तो ठीक है। विद्वता दिखानेके लिये उनको परास्त करनेके लिये, दम्भके लिये अपनेको महात्मा प्रदर्शित करनेके लिये पूछना ठीक नहीं है। आत्माके हितके लिये पूछना लाभप्रद है। दूसरे कारणसे पूछना ठीक नहीं है।
सत्संगमें कोशिश तो यही रखनी चाहिये कि कीमती बात हो। कोई कम कीमती बात भी हो तो उसकी कीमती मान लें। जिसका सत्संगमें प्रेम होता है, उसके लिये बेकीमती बात होती ही नहीं, सब कीमती ही होती है। श्रद्धा-प्रेमवालेको जो कुछ क्रिया देखनेमें आती है, उसे देखकर उसके प्रसन्नता, आनन्द, सुख, शान्तिका ठिकाना नहीं रहता। बहुत श्रद्धावाला तो यह बात सुनकर हँसता है कि देखो ये लोग कीमती बातको समझ नहीं रहे हैं। मुझे कितना आनन्द हो रहा है, कितनी प्रसन्नता, शान्ति हो रही है। यदि कीमती नहीं होती तो मुझे कैसे इतनी प्रसन्नता आदि होती। गोपियोंकी दृष्टिमें भगवान् की सारी क्रिया महत्त्वकी थी। उठाकर खाना सब महत्त्वकी बात थी। सारी क्रियाएँ बहुत महत्त्व देनेवाली थीं। गौतमकी गायें चरानेकी आज्ञा सत्यकामके लिये महत्त्वकी बात थी। ४०० गायें ले जाकर वनमें चरानेकी गुरुकी आज्ञा उसकी दृष्टिमें गुरुकी कृपा थी। वह समझता था कि मेरे उद्देश्यकी पूर्ति इसीमें है। हम क्या जानें भगवान् कैसे मिलते हैं। राजपूतानेके लिये लोगोंको कितना कहते हैं कि गायोंकी सेवा करनी है, कौन सुनता है।
शुकदेवजी जनकके द्वारपर जाते हैं आज्ञा होती है खड़े रहने दो। शुकदेवजी शान्तचित्त सात दिनतक खड़े रहे, कोई विकार नहीं हुआ, शान्ति और आनन्द था। जानते थे यही आज्ञा ज्ञान देनेवाली है। श्रद्धालु पुरुषको श्रद्धेयकी सभी क्रिया ऊँचे दर्जेकी मालूम देती है। प्रेमीको प्रेमास्पदकी सारी क्रिया ऐसी ही मालूम देती है। ऊँचा-नीचा दर्जा दीखे तो यह प्रेमकी, श्रद्धाकी कमीका ही द्योतक है। श्रद्धालुकी दृष्टिमें बेदामी बात कभी होती ही नहीं। वहाँ कोई दर्जा भी नहीं है, वह तो दर्जेवाले पुरुषसे डरता है। कहीं तेरेपर उसका भाव न आ पड़े। उसके तो उत्तरोत्तर आनन्द और शान्ति समाती ही नहीं। प्रत्येक क्रियामें न्याय, प्रेम तथा संसारका उद्धार दीखता है। उसकी दृष्टिमें कोई ऊँचे-नीचे दर्जेकी बात ही नहीं है। भोजन करना, सोना, पेशाब करना सबमें ऊँचा-ही-ऊँचा दीखता है। उसे तो हँसी आती है कि गंगाके किनारे लोग प्यासे मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और गंगा बह रही है। कारण यह है कि गंगाकी तरफ पीठ दे रखी है, अन्धे हैं प्रेममयी, शान्तिमयी और आनन्दमयी गंगा बह रही है। श्रद्धा और प्रेमरूपी दो नेत्र हैं। जिसके न हों वह अन्धा है, एक हो तो भी दीखे, कानेको भी दीखता है। दोनों फूट जायँ तो नहीं दीखता।
यह बात सच्चे महापुरुषों के विषय में कही गयी और जो सच्चे जिज्ञासु हैं उनके लिये कही गयी। अपने लिये तो प्रेम प्रभावकी बात एक नम्बरकी, पीड़ितोंकी सेवा, गायोंकी सेवा दो नम्बरकी तथा घरमें सबको प्रसन्न रखना तथा रोजगारकी बात तीन नम्बर है। भक्त के लिये क्रिया मूल्यवान् होती है। एक ही बात पचास आदमी सुनते हैं। सब अपने अपने भावके अनुसार करते हैं। सबपर अलग-अलग असर है। एक ही देश, एक ही काल, एक ही व्यक्ति, वही बातें, सबपर एक-सा असर नहीं पड़ता। आकाशसे एक ही कालमें एक ही खेतमें जल पड़ता है। जितने पौधे हैं अलग-अलग असर होता है। वही जल साँपपर पड़कर विष, आमपर रस, बबूलपर काँटा हो जाता है। बीजके भेदसे अलग-अलग असर होता है। मिट्टीमें कोई भेद नहीं। जलमें भेद नहीं है, बीजके भेदसे अलग-अलग असर है। आपकी दृष्टिसे दामी बात हो गयी। वास्तव में बात समझमें आ जाय तो दामी-बेदामीका भेद मिट जाय। दामीके सिवाय बेदामी हो ही नहीं। आप चाहते हैं थोड़ी देर दामी बातें होनी चाहिये तो बाकी तो फिर बेदामी ही हुई। अपना तो साराका–सारा समय दामी ही बीतना चाहिये। बहुत जल्दी भगवत्प्राप्ति हो जायगी तो क्या हर्ज है बाकीका समय दूसरोंके काममें आवे। शेषके लिये रख छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। जितने धनकी जरूरत है उससे ज्यादा होगा वह और भाइयोंके काम आयेगा। जल्दी-से-जल्दी काम हो जाय, मृत्युका क्या भरोसा है। वही सबसे बढ़कर बुद्धिमान् है जिसका एक क्षण भी बेदामी नहीं बीतता, यह अपने हाथकी बात है। भगवान्, सन्त और महात्माओंके पास तो कोई कमी है नहीं। उनकी शक्तिकी कमी तो होती नहीं है वे दयाके सागर हैं। पारसके छूनेसे सोना होते-होते शायद कभी पारस समाप्त हो जाय पर प्रभुकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे दयाके समुद्र हैं। वहाँ कोई कमी नहीं है। बुद्धि माँगे तो बुद्धि, योगक्षेम माँगे तो योगक्षेम देते हैं जो माँगे सो देनेकी उनकी घोषणा है, प्रतिज्ञा है। लेनेमें भी परिश्रम नहीं है सुसुखं कर्तमव्ययम्। लगातार धारा प्रवाह दे रहे हैं। पर पात्र हमारे पास नहीं है। हजारों छेदोंवाली चलनी लिये बैठे हैं। पहाड़से धार गिर रही है। बीचमें खाईं है इसलिये अंजलिमें नहीं ले जाता है। रास्तेमें खाई लाँघना कठिन है।
दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।।
(गीता ७।१४)
यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लङ्कन कर जाते हैं अर्थात् संसारसे तर जाते हैं।
खड़े होकर पुकारें उनकी तो घोषणा है-
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्।
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्।।
(गीता १२।७)
हे अर्जुन! उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ।
हम भयसे नहीं लाँघते है। प्रभु कहते हैं मैं झट पकड़ लूंगा पर हमलोग लाँघते ही नहीं है। लाँघते ही तो शान्ति और आनन्दका समुद्र है। हमलोग दूरसे ही लेते हैं। चलनीमें भी यदि पता लगा दें तो हमारे लायक जल तो आ ही जाय। अन्त:करण चलनी है। नि:स्वार्थभाव पता है। जितना-जितना नि:स्वार्थ है उतना-उतना जल मिलता ही है। जितना-जितना निष्काम भाव है उतनी-उतनी ही शान्ति है। श्रद्धा, प्रेम, नि:स्वार्थ भाव सब वृक्ष हैं पासमें खड़े हैं। पत्ते तोड़कर लाकर चलनीमें लगा दो बस प्यास बुझाने लायक जल मिल जायगा।
|
|||||
- सत्संग की अमूल्य बातें